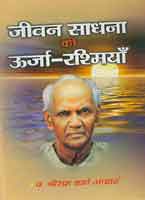|
आचार्य श्रीराम शर्मा >> स्रष्टा का परम प्रसादःप्रखर प्रज्ञा स्रष्टा का परम प्रसादःप्रखर प्रज्ञाश्रीराम शर्मा आचार्य
|
207 पाठक हैं |
||||||
स्रष्टा का परम प्रसाद....
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
सार-संक्षेप
मानवीय अंतराल में प्रसुप्त पड़ा विभूतियों का सम्मिश्रण जिस किसी में
सघन- विस्तृत रूप में दिखाई पड़ता है, उसे प्रतिभा कहते हैं। जब इसे
सदुद्देश्यों के लिए प्रयुक्त किया जाता है तो यह देवस्तर की बन जाती है।
और अपना परिचय महामानवों जैसा देती है। इसके लिए विपरीत यदि मनुष्य इस
संपदा का दुरुपयोग अनुचित कार्यों में करने लगे तो वह दैत्यों जैसा
व्यवहार करने लगती है। जो व्यक्ति अपनी प्रतिभा जो जगाकर लोकमंगल में लगा
देता है, वह दूरदर्शी और विवेकवान् कहलाता है।
आज कुसमय ही है कि चारों तरफ दुर्बुद्धि का साम्राज्य छाया दिखाई देता है। इसी ने मनुष्य को वर्जनाओं को तोड़ने के लिए उद्धत स्वभाव वाला वनमानुष बनाकर रख दिया है।
दुर्बुद्धि ने अनास्था को जन्म दिया है एवं ईश्वरीय सत्ता के संबंध में भी नाना प्रकार की भ्रांतियाँ समाज में फैल गई हैं। हम जिस युग में आज रह रहे हैं, वह भारी परिवर्तनों की एक श्रृंखला से भरा है। इसमें अनेक परिष्कृत प्रतिभाओं के उभरकर आने व आत्मबल उपार्जित कर लोकमानस की भ्रांतियों को मिटाने की प्रक्रिया द्रुतगति से चलेगी। यह सुनिश्चित है कि युगपरिवर्तन प्रतिभा ही करेगी। मनस्वी-आत्मबलसंपन्न ही अपनी भी- औरों की भी नैया खेते देखे जाते हैं। इस तरह सद्बुद्धि का उभार जब होगा तो जन-जन के मन-मस्तिष्क पर छाई दुर्भावनाओं का निराकरण होता चला जाएगा। स्रष्टा की दिव्यचेतना का हर परिष्कृत अंत:करण में होगा एवं देखते-देखते युग बदलता जाएगा। यही है प्रखर प्रज्ञारूपी परमप्रसाद जो स्रष्टा- नियंता अगले दिनों सुपात्रों पर लुटाने जा रहे हैं।
आज कुसमय ही है कि चारों तरफ दुर्बुद्धि का साम्राज्य छाया दिखाई देता है। इसी ने मनुष्य को वर्जनाओं को तोड़ने के लिए उद्धत स्वभाव वाला वनमानुष बनाकर रख दिया है।
दुर्बुद्धि ने अनास्था को जन्म दिया है एवं ईश्वरीय सत्ता के संबंध में भी नाना प्रकार की भ्रांतियाँ समाज में फैल गई हैं। हम जिस युग में आज रह रहे हैं, वह भारी परिवर्तनों की एक श्रृंखला से भरा है। इसमें अनेक परिष्कृत प्रतिभाओं के उभरकर आने व आत्मबल उपार्जित कर लोकमानस की भ्रांतियों को मिटाने की प्रक्रिया द्रुतगति से चलेगी। यह सुनिश्चित है कि युगपरिवर्तन प्रतिभा ही करेगी। मनस्वी-आत्मबलसंपन्न ही अपनी भी- औरों की भी नैया खेते देखे जाते हैं। इस तरह सद्बुद्धि का उभार जब होगा तो जन-जन के मन-मस्तिष्क पर छाई दुर्भावनाओं का निराकरण होता चला जाएगा। स्रष्टा की दिव्यचेतना का हर परिष्कृत अंत:करण में होगा एवं देखते-देखते युग बदलता जाएगा। यही है प्रखर प्रज्ञारूपी परमप्रसाद जो स्रष्टा- नियंता अगले दिनों सुपात्रों पर लुटाने जा रहे हैं।
चेतना की सत्ता एवं उसका विस्तार
इस संसार में जड़ के साथ चेतन भी गुथा हुआ है। काम करती तो काया भी दीखती
है, पर वस्तुत: उसके पीछे सचेतन की शक्ति काम कर रही होती है। प्राण निकल
जाए तो अच्छी-खासी काया निर्जीव हो जाती है। कुछ करना-धरना तो दूर, मरते
ही सड़ने-गलने का क्रम आरंभ हो जाता है और बताता है कि उसके साथ ईश्वरीय
चेतना जुड़ी रहती है। दोनों के पृथक होते ही समूचे खेल का अंत हो जाता है।
एकाकी चेतना का अपना अस्तित्व तो है। उसकी निराकार सत्ता सर्वत्र समाई हुई है। साकार होती तो किसी एक स्थान पर, एक नाम-रूप के बंधन में बँधकर रहना पड़ता और वह ससीम बनकर रह जाती। इसलिए उसे भी अपनी इच्छित गतिविधियाँ चलाने के लिए किन्हीं शरीर कलेवरों का आश्रय लेना पड़ता है। इस प्रकार प्रत्यक्ष परिचय प्राप्त करना संभव है। निराकार तो प्रकृति की लेसर, एक्स-किरणें आदि अनेक धाराएँ काम करती हैं, पर उनको समझ सकना खुली आँखों से नहीं वरन् किन्हीं सूक्ष्म उपकरणों के सहारे भी संभव हो पाता है। गाड़ी के दो पहिए मिल-जुलकर ही काम चलाते हैं। इसी प्रकार इस संसार की विविध गतिविधियाँ विशेषत: प्राणिसमुदाय की इच्छित हलचलों के पीछे अदृश्य सत्ता ही काम करती है, जिसे ईश्वर आदि नामों से जाना जाता है।
विराट् ब्रह्मांड में संव्याप्त सत्ता को विराट् ब्रह्म या परमात्मा कहते हैं। वही सर्वव्यापी, न्यायकर्त्ता, सत्-चित्-आनंद आदि विशेषणों से जाना जाता है। उसी का एक छोटा अंश जीवधारियों के भीतर काम करता है। मनुष्य में इस अंश का स्तर ऊँचा भी है और अधिक भी, इसलिए उसके अंतराल में अनेक विभूतियों की सत्ता प्रसुप्त रूप में विद्यमान पाई जाती है। यह अपने निजी पुरुषार्थ के ऊपर अवलंबित है कि उसे विकसित किया जाए या ऐसे ही उपेक्षित रूप में-गई गुजरी स्थिति में वहीं पड़ी रहने दिया जाए।
इस सम्मिश्रण का जहाँ भी अपेक्षाकृत अधिक विस्तृत स्वरूप दिखाई पड़ता है, उसे प्रतिभा कहते हैं। सदुद्देश्यों के लिए प्रयुक्त किए जाने पर यही प्रतिभा देव-स्तर की बन जाती है और अपना परिचय महानुभावों जैसा देती है, किन्तु साथ ही यदि मनुष्य अपनी उपलब्ध स्वतंत्रता का उपयोग अनुचित कामों में करने लगे तो वह दुरुपयोग ही दैत्य बन जाता है। दैत्य अपने और अपने संपर्क वालों के लिए विपत्ति का कारण ही बनते हैं; जबकि देवता पग-पग पर अपनी शालीनता और उदारता का परिचय देते हुए अपने प्रभाव-क्षेत्र में सुख, शांति एवं प्रगति का वातावरण बनाते रहते हैं। दैत्य-स्तर के अभ्यास बन जाने पर तो पतन और पराभाव ही बन पड़ता है। उसमें तात्कालिक लाभ दीखते हुए भी अंतत: दुर्गुणों का दुष्परिणाम ही प्रत्यक्ष होता है।
सृष्टि के नियम में कर्म और फल के बीच कुछ समय लगने का विधान है। बाज बोने पर उससे वृक्ष बनने में कुछ समय लग जाता है। गर्भाधान के कई मास बाद बच्चा उत्पन्न होता है। आज का दूध कहीं कल जाकर दही बनता है। अभक्ष्य खा लेने पर दस्त-उल्टी आदि होने का सिलसिला कुछ समय बाद आरंभ होता है। मनुष्यों में यह बालबुद्धि देखी जाती है कि वे तत्काल कर्मफल चाहते हैं, देर लगने पर अधीर हो जाते है और चाहते हैं कि हथेली पर सरसों जमे; कल तक उसमें पौधे जमने की प्रतीक्षा न करनी पड़े। उतावली आतुरता उत्पन्न करती है मन:स्थिति प्राय: अद्धविक्षिप्त की-सी बना देती है, जिसमें तात्कालिक लाभ भर दीख पड़ता है; चाहे वह कितना ही क्षणिक या दु:खदायी ही क्यों न हो। वह विवेकवान् दूरदर्शिता न जाने कहाँ चली जाती है जिसे अपनाकर विद्यार्थी विद्वान्, दुबले पहलवान, मंदबुद्धि तीव्रबुद्धि एवं पिछड़े धनवान बनते हैं। यह एक ही मनुष्य की प्रधान भूल है, जिसके कारण वह अपने जीवन का उद्देश्य, स्वरूप और वरिष्ठता तक भूल जाता है- मार्ग से भटककर झाड़-झँखाड़ों में पड़ता है कि ‘‘मनुष्य वस्तुत: ईश्वर की संतान तो है ही नहीं वरन् डार्विन के कथनानुसार वह बंदर की ही अनगढ़ औलाद है।’’
यह व्यंग्य-उपहास मनुष्य के अचिंत्य चिंतन का है। इसी के कारण उसके चरित्र और व्यवहार में भ्रष्टता घुस पड़ती है। और तरह-तरह के आक्षेप-उलाहना लगने शुरू होते हैं। दुष्ट चिंतन की भ्रष्ट आचरण का निमित्त बनता है और इसी के कारण अनेक अवांछनीयताएँ उसके सिर पर लद लेती हैं। कहना न होगा कि कर्मफल भोगे बिना किसी को छुटकारा नहीं; भले ही वह भटकाव के कारण ही क्यों न बन पड़ी हो। चारे के लोभ में चिड़ियाँ और मछलियाँ बहेलियों के हाथ पड़ती और अपनी जान गँवाती देखी गई हैं। जो बोया है वही तो काटना पड़ेगा; भले ही पीछे सतर्कता बरती गई हो या समझदारी से काम लिया गया हो।
यही है भ्रांति, विकृति और विपत्ति का केन्द्र। इसके भँवर में फँसकर अधिकांश लोग गर्हित गतिविधियाँ अपनाते और दुर्गति के भाजन बनते हैं। यदि इस भूल से बचा जा सके तो मनुष्य को ईश्वर का उत्तराधिकारी, ज्येष्ठ राजकुमार कहने में किसी को क्यों आपत्ति हो ? फिर उसकी प्रकृति स्वार्थी बनकर आनंद का रसास्वादन करते रहने में क्यों किसी प्रकार बाधक बने ? क्यों उसे वासना, तृष्णा और अहंता के लौहपाशों में जकड़ जाने पर वंदीगृह के कैदी जैसी विडंबनाएँ सहनी पड़ें ? क्यों मरघट में रहने वाले व्यक्तियों जैसा नीरस, निष्ठुर और हेय जीवन जीना पड़े ? क्यों डरती-डराती और रोती-रुलाती जिंदगी जीनी पड़े ?
इस संसार में अंधकार भी है और प्रकाश भी; स्वर्ग भी है और नरक भी; पतन भी है और उत्थान भी; त्रास भी है और आनंद भी। इन दोनों में जिसे चाहे, मनुष्य इच्छानुसार चुन सकता है। कुछ भी करने की सभी को छूट है, पर प्रतिबंध इतना ही है कि कृत्य के प्रतिफल से बचा नहीं जा सकता। स्रष्टा के निर्धारित क्रम को तोड़ा नहीं जा सकता। करने की छूट होते हुए भी उसे परिणाम भुगतने के लिए सर्वथा बाध्य रहना पड़ता है। यह दूसरी बात है कि इस प्रक्रिया के पकने में कुछ विलंब लगता है। मुकदमा दायर होने और सजा मिलने में अपने न्यायाधीश भी तो ढेरों समय लगा लेते हैं। ईश्वर का कार्यक्षेत्र तो और भी अधिक विस्तृत है।
उनके न्याय करने में यदि देर लग जाती है तो मनुष्य को धैर्य खोने की आवश्यकता नहीं है और न यह अनुमान लगाने की कि वहाँ अंधेरगरदी चलती है। चतुरता के बलबूते अपने यहाँ तो अनेक अपराधी दंड पाने से बच जाते हैं, पर सर्वव्यापी और सर्वसाक्षी न्यायाधीश के न्याय में किसी को ऐसे अवसर नहीं मिलते। इस वास्तविकता से असहमत रहने के कारण ही लोग प्राय: नास्तिक बन जाते हैं- कर्मफल की मान्यता का उपहास उड़ाते हुए स्वेच्छाचार बरततें हैं। विवेक होने की समझ तभी आती है जब समयानुसार क्रिया की प्रतिक्रिया सामने आ खड़ी होती है।
एकाकी चेतना का अपना अस्तित्व तो है। उसकी निराकार सत्ता सर्वत्र समाई हुई है। साकार होती तो किसी एक स्थान पर, एक नाम-रूप के बंधन में बँधकर रहना पड़ता और वह ससीम बनकर रह जाती। इसलिए उसे भी अपनी इच्छित गतिविधियाँ चलाने के लिए किन्हीं शरीर कलेवरों का आश्रय लेना पड़ता है। इस प्रकार प्रत्यक्ष परिचय प्राप्त करना संभव है। निराकार तो प्रकृति की लेसर, एक्स-किरणें आदि अनेक धाराएँ काम करती हैं, पर उनको समझ सकना खुली आँखों से नहीं वरन् किन्हीं सूक्ष्म उपकरणों के सहारे भी संभव हो पाता है। गाड़ी के दो पहिए मिल-जुलकर ही काम चलाते हैं। इसी प्रकार इस संसार की विविध गतिविधियाँ विशेषत: प्राणिसमुदाय की इच्छित हलचलों के पीछे अदृश्य सत्ता ही काम करती है, जिसे ईश्वर आदि नामों से जाना जाता है।
विराट् ब्रह्मांड में संव्याप्त सत्ता को विराट् ब्रह्म या परमात्मा कहते हैं। वही सर्वव्यापी, न्यायकर्त्ता, सत्-चित्-आनंद आदि विशेषणों से जाना जाता है। उसी का एक छोटा अंश जीवधारियों के भीतर काम करता है। मनुष्य में इस अंश का स्तर ऊँचा भी है और अधिक भी, इसलिए उसके अंतराल में अनेक विभूतियों की सत्ता प्रसुप्त रूप में विद्यमान पाई जाती है। यह अपने निजी पुरुषार्थ के ऊपर अवलंबित है कि उसे विकसित किया जाए या ऐसे ही उपेक्षित रूप में-गई गुजरी स्थिति में वहीं पड़ी रहने दिया जाए।
इस सम्मिश्रण का जहाँ भी अपेक्षाकृत अधिक विस्तृत स्वरूप दिखाई पड़ता है, उसे प्रतिभा कहते हैं। सदुद्देश्यों के लिए प्रयुक्त किए जाने पर यही प्रतिभा देव-स्तर की बन जाती है और अपना परिचय महानुभावों जैसा देती है, किन्तु साथ ही यदि मनुष्य अपनी उपलब्ध स्वतंत्रता का उपयोग अनुचित कामों में करने लगे तो वह दुरुपयोग ही दैत्य बन जाता है। दैत्य अपने और अपने संपर्क वालों के लिए विपत्ति का कारण ही बनते हैं; जबकि देवता पग-पग पर अपनी शालीनता और उदारता का परिचय देते हुए अपने प्रभाव-क्षेत्र में सुख, शांति एवं प्रगति का वातावरण बनाते रहते हैं। दैत्य-स्तर के अभ्यास बन जाने पर तो पतन और पराभाव ही बन पड़ता है। उसमें तात्कालिक लाभ दीखते हुए भी अंतत: दुर्गुणों का दुष्परिणाम ही प्रत्यक्ष होता है।
सृष्टि के नियम में कर्म और फल के बीच कुछ समय लगने का विधान है। बाज बोने पर उससे वृक्ष बनने में कुछ समय लग जाता है। गर्भाधान के कई मास बाद बच्चा उत्पन्न होता है। आज का दूध कहीं कल जाकर दही बनता है। अभक्ष्य खा लेने पर दस्त-उल्टी आदि होने का सिलसिला कुछ समय बाद आरंभ होता है। मनुष्यों में यह बालबुद्धि देखी जाती है कि वे तत्काल कर्मफल चाहते हैं, देर लगने पर अधीर हो जाते है और चाहते हैं कि हथेली पर सरसों जमे; कल तक उसमें पौधे जमने की प्रतीक्षा न करनी पड़े। उतावली आतुरता उत्पन्न करती है मन:स्थिति प्राय: अद्धविक्षिप्त की-सी बना देती है, जिसमें तात्कालिक लाभ भर दीख पड़ता है; चाहे वह कितना ही क्षणिक या दु:खदायी ही क्यों न हो। वह विवेकवान् दूरदर्शिता न जाने कहाँ चली जाती है जिसे अपनाकर विद्यार्थी विद्वान्, दुबले पहलवान, मंदबुद्धि तीव्रबुद्धि एवं पिछड़े धनवान बनते हैं। यह एक ही मनुष्य की प्रधान भूल है, जिसके कारण वह अपने जीवन का उद्देश्य, स्वरूप और वरिष्ठता तक भूल जाता है- मार्ग से भटककर झाड़-झँखाड़ों में पड़ता है कि ‘‘मनुष्य वस्तुत: ईश्वर की संतान तो है ही नहीं वरन् डार्विन के कथनानुसार वह बंदर की ही अनगढ़ औलाद है।’’
यह व्यंग्य-उपहास मनुष्य के अचिंत्य चिंतन का है। इसी के कारण उसके चरित्र और व्यवहार में भ्रष्टता घुस पड़ती है। और तरह-तरह के आक्षेप-उलाहना लगने शुरू होते हैं। दुष्ट चिंतन की भ्रष्ट आचरण का निमित्त बनता है और इसी के कारण अनेक अवांछनीयताएँ उसके सिर पर लद लेती हैं। कहना न होगा कि कर्मफल भोगे बिना किसी को छुटकारा नहीं; भले ही वह भटकाव के कारण ही क्यों न बन पड़ी हो। चारे के लोभ में चिड़ियाँ और मछलियाँ बहेलियों के हाथ पड़ती और अपनी जान गँवाती देखी गई हैं। जो बोया है वही तो काटना पड़ेगा; भले ही पीछे सतर्कता बरती गई हो या समझदारी से काम लिया गया हो।
यही है भ्रांति, विकृति और विपत्ति का केन्द्र। इसके भँवर में फँसकर अधिकांश लोग गर्हित गतिविधियाँ अपनाते और दुर्गति के भाजन बनते हैं। यदि इस भूल से बचा जा सके तो मनुष्य को ईश्वर का उत्तराधिकारी, ज्येष्ठ राजकुमार कहने में किसी को क्यों आपत्ति हो ? फिर उसकी प्रकृति स्वार्थी बनकर आनंद का रसास्वादन करते रहने में क्यों किसी प्रकार बाधक बने ? क्यों उसे वासना, तृष्णा और अहंता के लौहपाशों में जकड़ जाने पर वंदीगृह के कैदी जैसी विडंबनाएँ सहनी पड़ें ? क्यों मरघट में रहने वाले व्यक्तियों जैसा नीरस, निष्ठुर और हेय जीवन जीना पड़े ? क्यों डरती-डराती और रोती-रुलाती जिंदगी जीनी पड़े ?
इस संसार में अंधकार भी है और प्रकाश भी; स्वर्ग भी है और नरक भी; पतन भी है और उत्थान भी; त्रास भी है और आनंद भी। इन दोनों में जिसे चाहे, मनुष्य इच्छानुसार चुन सकता है। कुछ भी करने की सभी को छूट है, पर प्रतिबंध इतना ही है कि कृत्य के प्रतिफल से बचा नहीं जा सकता। स्रष्टा के निर्धारित क्रम को तोड़ा नहीं जा सकता। करने की छूट होते हुए भी उसे परिणाम भुगतने के लिए सर्वथा बाध्य रहना पड़ता है। यह दूसरी बात है कि इस प्रक्रिया के पकने में कुछ विलंब लगता है। मुकदमा दायर होने और सजा मिलने में अपने न्यायाधीश भी तो ढेरों समय लगा लेते हैं। ईश्वर का कार्यक्षेत्र तो और भी अधिक विस्तृत है।
उनके न्याय करने में यदि देर लग जाती है तो मनुष्य को धैर्य खोने की आवश्यकता नहीं है और न यह अनुमान लगाने की कि वहाँ अंधेरगरदी चलती है। चतुरता के बलबूते अपने यहाँ तो अनेक अपराधी दंड पाने से बच जाते हैं, पर सर्वव्यापी और सर्वसाक्षी न्यायाधीश के न्याय में किसी को ऐसे अवसर नहीं मिलते। इस वास्तविकता से असहमत रहने के कारण ही लोग प्राय: नास्तिक बन जाते हैं- कर्मफल की मान्यता का उपहास उड़ाते हुए स्वेच्छाचार बरततें हैं। विवेक होने की समझ तभी आती है जब समयानुसार क्रिया की प्रतिक्रिया सामने आ खड़ी होती है।
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book


 i
i